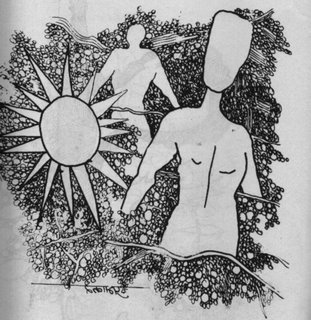(निर्धारण एवं क्रियान्वयन)
इतिहास साक्षी है कि किसी भी ताकत से लड़ने के लिए संगठित होना आवश्यक है। अंग्रेजों की ताकत से लड़ने के लिए गाँधी जी ने सबको संगठित किया था। स्वतंत्रता का बिगुल बजाने वाले मंगल पांडे की आहुति भी तब ही सार्थक हुई जब तत्कालीन राजा महराजाओं ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई आज की अंग्रेजी वर्चस्व की ताकत अंग्रेजों के शासन की ताकत से कहीं अधिक शक्तिशाली है और अंग्रेजी माध्यम की स्कूली शिक्षा से यह ताकत घर घर में बढ़ती जा रही है।
स्वतंत्रता के बाद स्वार्थवश अंग्रेजी के पक्षधरों द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग की दी गई छूट के कारण आज की स्थिति पैदा हुई है और उनकी कथनी और करनी में अंतर के कारण स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। दिखाने के लिए भारतीय सत्ताधारी राजनेताओं ने भारतीय भाषाओं भाषाओं को राजभाषा का दर्जा तो दे दिया है और हिन्दी दिवस पर वे एवं सत्ताधारी बुध्दिजीवी हिन्दी के गुणगान करते नहीं थकते और उसके प्रचार के लिए करोडों रुपयों का अनुदान देते हैं, पर स्वयं उसका प्रयोग नहीं करते। इसी कारण हिन्दी ही नहीं अन्य भारतीय भाषाएँ भी अंग्रेजी के आगे बौनी पड़ गई हौ। परिणाम स्वरूप आज आधी सदी के बाद भी राष्ट्र गूँगा है और उसकी कोई पहचान नहीं है, कोई भी भाषा राष्ट्र की सम्पर्क भाषा घोषित नहीं हुई है। हिन्दी जब अपने ही प्रदेश में प्रतिष्ठापित नहीं हुई है तो उसे राष्ट्र की संपर्क राष्ट्रभाषा बनाने का सपना भी पूरा नहीं हो सकता। प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी के वर्चस्व से कौन पीड़ित या व्यथित है- व्यक्ति या राष्ट्र या कोई नहीं; यदि नहीं तो चिंतन व्यर्थ है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस विषय पर गंभीरता से चिंतन करें अब तक के प्रयासों एवं अनुभवों के आधार पर संयुक्त कार्य योजना तैयार करें और क्रियान्वयन की समयबद्ध रूप रेखा निर्धारित करें।
संयुक्त प्रयास पर चिंतन करने के लिए 1995 में लगभग 10 संस्थाओं ने मिल कर नागदा में भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद का गठन किया था। इसका लक्ष्य एक अलग संस्था का गठन करना नहीं वरन् सभी संबद्ध संस्थाओं की एक कार्यकारिणी परिषद के रूप में कार्य करना था। अप्रैल सन् 2003 में ठाणे महाराष्ट्र में इसका पंजीकरण कराया गया। मुंबई,दिल्ली, भोपाल,सतना,चैन्नई एवं चित्रकूट में चिंतन रैली, एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इस परिषद के माध्यम से जगह जगह से राष्ट्रपति जी को गणतंत्र दिवस पर संदेश स्वभाषा या हिन्दी में देने के लिए पत्र भिजवाए । 2 अक्टूबर 2003 को गाँधी के विचारों पर आधारित भाषा नीति के महत्व को समझाने के लिए जगह जगह जन चेतना अभियान किया गया। इन प्रयासों के दौरान निम्नलिखित अनुभव हुएः-
जनता की उदासीनता स्पष्ट महसूस हुई, अंग्रेजी बिना वे अपने को हीन महसूस करते हैं
लोग कहते हैं कि हिन्दी है तो सही पर वे नहीं समझते कि बोलने वाली भाषा का कोई महत्व नहीं है
संगोष्ठियों में सब मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम स्वभाषा हो पर क्रियान्वयन पर अटक जाते हैं।
मुंबई में एक जनमत सर्वेक्षण में अधिकतर ने हिन्दी को सम्पर्क राष्ट्रभाषा माना पर सत्ताधारी लोगों का कहना है कि यदि हिन्दी पहले ही राष्ट्रभाषा बन जाती तो ठीक रहता पर, अब संभव नहीं है, अब अंग्र्रेजी के वर्चस्व को हटाना कठिन है।
प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयंत नार्लीकर का मानना है कि सबकी स्कूली शिक्षा स्वभाषा से हो और उच्च शिक्षा अंग्रेजी से हो, पर पूछने पर कि इसको क्रियान्वित कैसे करेंगे, उनके पास कोई उत्तर नहीं था।
गैर हिन्दी भाषी क्या हमारे सत्ताधारी हिन्दी भाषी भी अंग्रेजी को 'कॉमन भाषा 'मानते हैं और हिन्दी का अपमान हो रहा है इस पर कोई चिंतन नहीं करते।
भारतीय भाषाओं का विकास बोलने की दिशा में हुआ है और हम केवल उपभोक्ता बनते जा रहे हैं।
दक्षिण भारत में हिन्दी के लिए निजी तौर पर हिन्दी अध्यापन का कार्य किया जा रहा है क्योंकि अन्य राज्यों में आवागमन के लिए यह जरूरी है, सम्पर्क राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी उन्हें स्वीकार नहीं।
वोट माँगने, धनोपार्जन, विज्ञापन,मनोरंजन के लिए स्वभाषा स्वीकृत है, पर लिखने पढ़ने के लिए नहीं।
संसद में भारतीय भाषाओं में बोलने का प्रावधान होते हुए भी राजनेता अंग्रेजी में बोलते हैं।
स्वदेशी की आवाज उठाने वाले भी स्वभाषा की आवाज नहीं उठाते।
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि हमारे सत्ताधारी प्रशासनिक, वैज्ञानिक एवं राजनेता इस तथ्य को या तो समझ नहीं रहे हैं या समझ कर भी अनदेखा कर रहे हैं। यही कारण है कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सत्ता पाने के बाद बदल गए। हमारे आध्यात्मिक गुरु भी इस तथ्य को न समझने के कारण अपने प्रवचनों में इसका चिंतन नहीं फैलाते।
विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठियों /सम्मेलनों/हिन्दी दिवस पर हिन्दी की गुणवत्ता पर पर्याप्त चिंतन और राष्ट्रीय स्तर पर उसे स्वीकार कराने के लिए देवनागरी लिपि में सुधार करने पर चर्चा हुई है, परन्तु हकीकत में राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनने में होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए कोई जमीनी कार्यक्रम निर्धारित नहीं किया गया। इस विषय पर भी चर्चा नहीं हुई कि भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठापन क्यों आवश्यक है और कैसे सुनिश्चित किया जाए।
स्वभाषा के महत्व को समझने वालों में कुछ करने की उमंग उठती है पर फिर निराशा से समाप्त होजाती है जैसे पानी में बबूले उठते हैं और खत्म हो जाते हैं, चिंगारी उठती हैं और बुझ जाती हैं।
अंग्रेजी की मानसिक गुलामी की पराकाष्ठा यह है कि मिशनरी के स्कूलों में हिन्दी बोलने पर सजा को अभिवावक केवल अनदेखा ही नहीं कर रहे हैं वरन् स्कूल प्रशासन से इस बार में सहमत होते हैं।
विश्व में स्वभाषा का स्वाभिमान रखने वाला हर व्यकित अपने परिचय पत्र में स्वभाषा को अवश्य स्थान देता है, पर हमारे देश की युवा पीय्ढी ऐसा नहीं मानती। उसके शब्दकोष में पहचान शब्द नहीं है। यह बात यह दर्शाती है कि हम गुलाम हैं क्योंकि गुलाम की ही कोई पहचान नहीं होती।
उपर्युक्त अनुभवों के आधार पर एक निश्चित दिशा में जाने के लिए 'भारतीय भाषाओं का प्रतिष्ठापन क्यों और कैसे' विषय पर पिछले वर्ष गाजियाबाद में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था और विभिन्न दृष्टिकोणों यथा भावनात्मक, सांस्कृतिक, राष्ट्र एवं जन हित, तथा व्यक्तिगत स्वार्थ एवं रोजी रोटी की दृष्टि से चर्चा की गई। अब आगरा में 23 अप्रैल को केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में भारतीय भाषाओं के प्रतिष्ठापनार्थ संयुक्त कार्य योजना का निर्धारण एवं क्रियान्वयन की समयबद्ध रूप रेखा तैयार की जाएगी। विभिन्न दृष्टिकोण में विचारणीय बिन्दु इस प्रकार हैं:-
भावनात्मकः- इसमें विचारणीय है स्वभाषा का मान-सम्मान। हमें स्वभाषा के सम्मान के लिए कार्य करना चाहिए और अपमान से बचाना चाहिए। कोई भाषा सम्मानित तब होती है जब वह ज्ञान विज्ञान की वाहक हो और अपमानित तब होती है जब उसका प्रयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाए जिसके लिए उसको निर्धारित किया गया है। अंग्रेजों के शासनकाल में हमारी भाषाएँ न सम्मानित थीं और न हीं अपमानित होती थीं पर अब अपमानित भी हो रही हैं। आज हमारी भारतीय भाषाएँ राज्यभाषाएँ एवं राजभाषा बनी हुई हैं पर हकीकत में उनको यह दर्जा प्राप्त नहीं है, अतः वे अपमानित हो रही हैं। सबसे अधिक अपमानित हिन्दी है। इसका कारण स्वभाषा के स्वाभिमान का विलुप्त हो जाना है। अतः स्वभाषा को सम्मान दिलाना या उन्हें अपमान से बचाने के लिए स्वभाषा के प्रति खोए स्वाभिमान को जगाना होगा।
सांस्कृतिकः- विचारणीय है कि संस्कृति क्या है और स्वभाषा व संस्कृति का क्या संबंध है? क्या यह अध्यात्मवाद एवं अपनापन है या हमारे ग्रंथ रामायण, गीता या पूजा पाठ ? प्रतिष्ठित पत्रकार डॉ झुनझुनवाले का कहना है कि अपने ग्रंथों का अंग्रेजीकरण कर दिया जाए तो हमारी संस्कृति बरकरार रहेगी। हाल में कल्याण के एक प्रकाशक ने हनुमान चालीसा को रोमन में निकालने का निर्णय लिया है।अंग्रेजी के किस स्तर के प्रयोग से संस्कृति नष्ट हो रही है ? अंग्रेजों के शासन काल में जब अंग्रेजी राजभाषा थी तब संस्कृति को इतना खतरा क्यों नहीं था ? हमारी भारतीय भाषाओं की मूल प्रवृति अध्यात्मवाद एवं अपनापन है जब कि अंग्रेजी की मूल भावना भौतिकवाद एवं औपचारिकता है। अंग्रेजों के समय में हमारी स्कूली शिक्षा स्वभाषा के माध्यम से होती थी और निजी व्यवहार, जैसे विवाह इत्यादि के निमन्त्रण पत्र, में स्वभाषा का प्रयोग होता था, पर आज अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दिन प्रतिदिन बढोत्तरी हो रही है और निजी व्यवहार में भी उसका प्रयोग बय्ढ रहा है। निजी व्यवहार को रोकने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले के साथ असहयोग करना होगा, जैसे अंग्रेजी में आए निमन्त्रणों को स्वीकार नहीं करना और स्वभाषा के प्रति स्वाभिमान को जगाना होगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को रोकने के लिए आगे विचार प्रस्तुत करेंगे।
राष्ट्र एवं जन हितः- किसी भी राष्ट्र एवं उसके जन हित का अर्थ है जन जन की खुशहाली,आर्थिक सम्पन्नता,आत्मनिर्भरता एवं स्वाभिमान से जीना। विश्व में विकसित राष्ट्रों में ऐसा पाया जाता है। विचारणीय है कि विकसित राष्ट्र बनने में स्वभाषा / जनभाषा की क्या भूमिका है? यह देखा जा सकता है कि विश्व में विकसित राष्ट्र वही है जिसकी जनभाषा, शिक्षा का माध्यम व कार्यभाषा एक हो। वैज्ञानिक तर्क पर यह सही प्रतीत होता है। किसी भी देश का विकास मौलिक शोध एवं उस देश की धरती के संसाधनों से जुय्डे प्रौद्यौगिकी विकास के लिए अनुप्रयोगिक शोध पर निर्भर करता है।
वैज्ञानिक शोध दो प्रकार के होते हैं मौलिक जिसमें प्राकृतिक नियमों की मूलभूत खोज होती है और अनुप्रयोगिक जो देश विशेष के संसाधनों,पर्यावरण,जलवायु इत्यादि पर आधारित होते हैं। अनुप्रयोगिक शोध से ही देश विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास होता है। जहाँ मौलिक शोध से देश की आर्थिक सम्पन्नता व उसकी प्रतिभा बय्ढती है वहीं अनुप्रयोगिक शोध से आत्मनिर्भरता बय्ढती है। मौलिक शोध का ताजा उदाहरण बिल ग्रेट्स द्वारा व्यक्तिगत कम्प्यूटर सिध्दन्त का विकास है इससे अमरीका की सम्पन्नता बढ़ी। स्वभाषा के कम्प्यूटरों का विकास अनुप्रयोगिक शोध का उदाहरण है।
देश विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास से ही जन-जन के लिए उपयोगी व्यवसाय विकसित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए घरेलू उद्योग धंधे यथा कुम्हार का मिट्टी का कुल्लड़, कृषि का विकास। कुल्लड़ का कचरा प्रदूषण पैदा नहीं करता क्योंकि टूटने पर मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। हमारे देश में किसान गोबर की खाद का प्रयोग करते थे, जो धरती की उर्वरा शक्ति को नष्ट नहीं करती। रासायनिक खाद का उपयोग करके हम अपनी धरती की उर्वरा शक्ति को खो रहे हैं। यदि इस क्षेत्र में शोध किया जाता तो कुम्हार के कुल्लड़ को मजबूत किया जाता । कचरा आदि से रसायन रहित खाद का प्रयोग बढ़ाया जाता, तो गॉव-गाँव में व्यवसाय विकसित होते और शहर की ओर दौड़ कम होती। इसी प्रकार परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में धरती से जुड़े शोध का उदाहरण है थोरियम आधारित परमाणु बिजली घर का विकास क्योंकि हमारे देश में थोरियम का अथाह भंडार है, यूरेनियम का नहीं। अतः थोरियम के परमाणु बिजली घर का विकास हमें आत्मनिर्भर बनाएँगे जब कि यूरेनियम के परमाणु बिजली घरों से हम पश्चिम के विशेषकर अमरीका पर निर्भर रहेंगे। इसी परनिर्भरता के कारण शायद हम परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने को विवश हुए हैं।
मौलिक और अनुप्रयोगिक दोनों प्रकार के शोध देश की प्रतिभाओं द्वारा होते हैं। दोनों शोध के लिए पहली आवश्यकता है मौलिक/रचनात्मक चिंतन व लेखन एवं ज्ञान का आत्मसात करना, दूसरी आवश्यकता है भाषा पर अधिकार व तीसरी है अपने देश की आवश्यकताओं को समझना। प्रश्न उठता है कि क्या अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाली प्रतिभाएँ इस दिशा में कार्य कर सकेंगी?
मौलिक चिंतन एवं लेखनः- इसमें विचारणीय है कि क्या
(1) स्कूली विशेषकर प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या जनभाषा से अलग भाषा होने पर मौलिक चिंतन समाप्त हो जाता है क्योंकि उस भाषा को सीखने के लिए रटना पय्डता है और बौध्दिक विकास के प्रारम्भिक वर्ष दूसरी भाषा के सीखने में ही व्यतीत हो जाते हैं। जब कि स्वभाषा या जनभाषा से सहजता से ज्ञान अर्जित करने के कारण मानसिक विकास होता है, दूसरे विचारों की उड़ान सपनों में होती है और सपने स्वभाषा में ही देखे जाते हैं । मौलिक चिंतन के विकास के लिए सपनों की भाषा एवं शिक्षण भाषा का एक होना आवश्यक है।
(2) ज्ञान का आत्मसात स्वभाषा/जनभाषा से ही संभव है क्योंकि वह जनम से हमारी रग रग में बस जाती है।
(3) दूसरे की भाषा से हम ज्ञान प्राप्त तो कर सकते हैं पर ज्ञान का सृजन नहीं कर सकते।
(4) मौलिक लेखन के लिए विचारों को लिपिबद्ध करने के लिए आवश्यक इच्छा तब ही होगी जब मौलिक लेखन स्वभाषा या जनभाषा में हो।
भाषा पर अधिकारः- व्यक्ति चाहे जितना भी चिंतन करले यदि उसका भाषा पर अधिकार नहीं है तो न तो वह सत्साहित्य को ग्राह्य कर सकता है और न स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता है। अपने शोध को समझाने के लिए भाषा पर अधिकार की आवश्यकता होती है। विचारणीय है कि क्या शिक्षा का माध्यम और बोलचाल की भाषा अलग होने से अभिव्यक्ति प्रभावी होगी या हम आधे अधूरे रहेंगे। सत्य तो यह है कि न तो हम उन लोगो में प्रभावी होंगे जिनकी मातृभाषा हमारी स्कूली शिक्षा का माध्यम है और नही अपने लोगों में ।
देश की आवश्यकताओं को समझनाः- अनुप्रयोगिक शोध के लिए आवश्यक है उस देश की मूलभूत आवश्यकताओं को समझना, उसके संसाधनों, उसकी जलवायु एवं उसके परिवेश से परिचित होना। भारत का परिवेश गाँवों से है अतः गाँवों से जुड़ना आवश्यक है। विचारणीय है कि अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने वाले लोग हमारे गाँवों की स्थिषत दर्शाने वाले समाचार पत्रों एवं स्वभाषा में लिखे साहित्य को न पढ़ने के कारण हमारे गाँवों के परिवेश से न जुय्ड कर विदेशी परिवेश से जुड़ रहे हैं।
उपर्युक्त तथ्यों के पक्ष में यह सिद्ध है कि स्वचतंत्रता पूर्व जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होनें स्कूली शिक्षा स्वभाषा या जनभाषा से प्राप्त की। आज भी सर्वेक्षण करके देखा जा सकता है कि वैज्ञानिक संस्थानों में कार्यरत अधिकांश वैज्ञानिकों ने स्कूली शिक्षा स्वभाषा से प्राप्त की है। फिर भी आगे अंग्रेजी माध्यम के कारण अधिकतर शोध विदेशों की नकल हैं या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इतिहास साक्षी है कि ज्ञान-विज्ञान जनभाषा से अलग होने के कारण शोध कार्य करने में समय अधिक व्यतीत होता है। एक उदाहरण उस वैज्ञानिक का है जिसने आधुनिक शल्य चिकित्सा (वैसे शल्य चिकित्सा का विकास वैदिक काल में शु द्वारा हुआ था) का विकास किया हज्जाम था। उस समय उच्च ज्ञान विज्ञान ग्रीक भाषा में ही उपलब्ध था, इसलिए उसे अपने कार्य में अधिक समय लगा। इसी प्रकार प्रो. सत्येन्द्र बोस ने जब एम. एससी किया तब उस स्तर की पुस्तकें प्रैंच्च में उपलब्ध थी। अतः उन्हें प्रैंच्च सीखने के कारण समय लगाना पड़ा। इसके अलावा यदि जनभाषा में वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध है तो जिस प्रतिभा ने उच्च शिक्षण नहीं पाया वह भी स्वभाषा में उपलब्ध ज्ञान विज्ञान को पढ़ कर वैज्ञानिक शोध कर सकता है। वैज्ञानिक माइकल फैराडे की जिल्दसाजी की दुकान थी। वह उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय नहीं गया दुकान पर जिल्द के लिए आने वाली वैज्ञानिक पुस्तकें जो उसकी स्वभाषा में थी पढ़कर वैज्ञानिक बन गया।
लोकप्रिय वैज्ञानिक लेखन की आवश्यकता :- यह भी विचारणीय है कि जनसाधारण को अंधविश्वास से बचाने एवं राष्ट्र की वैज्ञानिक प्रगति का एहसास दिलाने के लिए लोकप्रिय वैज्ञानिक पुस्तकें व पत्र पत्रिकाएँ स्वभाषा में होना आवश्यक है। जनसाधारण को अनुवाद करके वैज्ञानिक जानकारी पहुँचाई जा सकती है पर लोकप्रिय पुस्तक या पत्रिका के लिए अनुवाद मौलिक जैसा होना चाहिए या लेखन ही मौलिक होना चाहिए। मौलिक जैसे अनुवाद के लिए अनुवादको हिन्दी व अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं पर अधिकार एवं विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं। यह निर्विवाद है कि साहित्यकार द्वारा लिखा लेख रोचक होगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जयन्त नार्लीकर ने एक लेख में कहा है- ‘विज्ञान के प्रसार में साहित्यकारों को भी आगे आना चाहिए। वैज्ञानिकों की अपेक्षा साहित्यकारों की लेखनी में अधिक ताकत होती है। मैं हिन्दी में विज्ञान लिख सकता हूँ पर एक साहित्यकार जैसी नहीं होगी ।‘ यह सत्य है एक वैज्ञानिक की सहायता से साहित्यकार द्वारा अच्छे लोकप्रिय वैज्ञानिक लेख लिखे जा सकते हैं। वैज्ञानिक की सहायता का अर्थ है हिन्दी में वैज्ञानिक सामग्री की उपलब्धता। इसका सका उदाहरण है कि परमाणु ऊर्जा से संबंधित वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध कराने पर मेरी साहित्यकार पत्नी डॉ प्रेम भार्गव ने रोचक ढ़ंग से परमाणु की आत्मकथा लिखी जो रक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत हुई और हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को पसंद आई।
विचारणीय है कि आज स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से पाने वाली प्रतिभा मौलिक चिंतन खोने एवं गाँवों से न जुड़ने के कारण देश के विकास के काम न आकर विदेशियों के काम आ रही हैं। साथ ही स्वभाषा माध्यम से पढ़ने से मौलिक चिंतन प्राप्त करने वाली और गाँवों से जुड़ी प्रतिभाएँ भी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में होने के कारण समान अवसर नहीं मिलने और स्वभाषा में उच्च ज्ञान विज्ञान उपलब्ध न होने के कारण देश के काम नहीं आ रही हैं। दोनों प्रकार की प्रतिभाएँ देश के विकास में काम न आकर विदेशियों के उपयोगी सिद्ध हो रही हैं और परिणाम स्वरूप वे आज हमारे अन्नदाता बन गए हैं और हम केवल उपभोक्ता बनते जा रहे हैं और बने हुए हैं।
स्वभाषा प्रतिष्ठापन के महत्व पर निर्णायक चिंतन के लिए-
(क) गोष्ठी का आयोजन किया जाए जिसमें हमारे राष्ट्रपति समेत सत्ताधारी वैज्ञानिक चिंतन करें कि राष्ट्र के विकास के लिए मौलिक चिंतन एवं मौलिक लेखन स्वभाषा में होना आवश्यक है। उसके लिए वैज्ञानिकों की क्षमता का मूल्यांकन स्वभाषा में लिखे शोध के आधार पर भी किया जाना चाहिए।
(ख) स्वभाषा के माध्यम से शिक्षा एवं धरती से जुड़े और गाँवो के विकास के लिए शोध का संस्थान स्थापित करके स्वभाषा के महत्व को सिद्ध करना होगा ।
(ग) गॉवों और स्वभाषा के विद्यालयों में पुस्तकालय खोलना एवं वहाँ तक स्वभाषा की पत्र पत्रिकाएँ तथा पुस्तकों को पहँचाना होगा ।
(घ) इस तथ्य को समझने वालों को एकजुट होकर वैज्ञानिक साहित्य तैयार करना होगा और इस तथ्य को समझने वालों से वार्षिक आय की कुछ प्रतिशत धनराशि एकत्रित करनी होगी।
व्यक्तिगत स्वार्थः- व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण न तो जन हित के बारे में सोचा जाता है और न हीं राष्ट्र हित के बारे में। व्यक्ति को जिस रास्ते आर्थिक लाभ होता है वही करता है। इसी दृष्टि से विचारणीय है कि बिना किसी प्रयास के अंग्रेजी के प्रयोग का प्रसार हो रहा है व प्रयास के बाबजूद हिन्दी या भारतीय भाषाओं के प्रयोग में गिरावट। हाँ बोलने वाली भाषा के रूप में अवश्य विस्तार है। व्यापारी हो या राजनेता या अभिनेता या उद्योगपति उसे किसी भाषा से मतलब नहीं। वह तो उसी भाषा का स्तेमाल करेगा जिससे उसका काम चलता है। हम देख सकते हैं-
राजनेताओं के लिए स्वभाषा 'वोट' के लिए, अंग्रेजी कामकाज के लिए
अभिनेताओं के लिए स्वभाषा से धनोपार्जन, अंग्रेजी फिल्म समारोह में अंग्रेजी का प्रयोग
उद्योगपतियों के लिए स्वभाषा से 'विज्ञापन', अंग्रेजी से नौकरी देना व कामकाज करना
व्यापारियों के लिए स्वभाषा से 'माल' बेचना, अंग्रेजी से नामपट,कैशमीमो लिखना व कामकाज करना
विवाह व अन्य समारोह में बोलचाल की भाषा स्वभाषा, पर निमन्त्रण पत्र व लिखने की भाषा अंग्रेजी
दक्षिण भारत में हिन्दी शिक्षण का कारोबार चल रहा है क्योंकि अधिकतर बाजार की भाषा हिन्दी है अतः उद्योग व व्यापार के क्षेत्र में जहाँ कार्यभाषा अंग्रेजी है बाजार के कारण हिन्दी का ज्ञान भी आवश्यक है। उत्पादों पर अंग्रेजी छाई हुई होती है। लोगों के द्वारा स्वभाषा का प्रयोग करवाने के लिए असहयोग आन्दोलन द्वारा स्वभाषा की आवश्यकता बढ़ाई जा सकती है।
रोजी रोटीः- मानव रोजी रोटी के लिए ही जीता है। अतः येन केन प्रकारेण रोजी रोटी के लिए जो भी आवश्यक है उसे करने पर वह मजबूर होता है। हिन्दी एवं भारतीय भाषाओं के लिए संघर्षरत भी अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिलवाते हैं। इसी विषय पर अदालत में हिन्दी के प्रयोग के लिए संघर्षरत एक सेवानिवृत न्याय मूर्ति ने कहा कि उनके बच्चे एवं पोता-पोती स्कूली शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से इसलिए पाते हैं जिससे उनका भविष्य सुधर जाए। उन्होंने यह नहीं कहा कि मजबूरी में भेजते हैं। विचारणीय है कि यदि अंग्रेजी माध्यम पैसे वालों के बच्चों का भविष्य सुधार सकता है तो गरीब तबके के बच्चों का भविष्य क्यों नहीं? स्वभाषा को रोजी रोटी से जोय्डने पर ही समस्या का समाधान संभव है। अतः पुरस्कार दी जाने वाली राशि को पहले लघु उद्योगों में लगाया जाए, फिर उनसे प्राप्त धन से बड़े उद्योग खोले जा सकते हैं ।
भाषा का कम्प्यूट्रीकरणः-आज कम्प्यूट्रीकरण का युग है अतः विचारणीय है कि क्या स्वभाषा के मानक कुजी पटल बिना और प्रत्येक कार्य के लिए सॉटवेयर विकसित हुए बिना हमारी भाषाओं में कार्य करना संभव है?
योजना तैयार करने के लिए यह भी विचारणीय है कि अब तक के प्रयास प्रभावी क्यों नहीं रहे। इनमें प्रमुख हैं-
(1) विभिन्न संस्थाओं द्वारा हिन्दी के प्रचार व प्रसार का अर्थ केवल हिन्दी की शिक्षा देना है, तो क्या इससे वह राजभाषा पद पर हकीकत में प्रतिष्ठापित हो सकेगी।
(2) इस अभियान में लगे व्यक्तियों के बच्चों का अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाना या विदेश में बसना।
(3) साल में एक बार सम्मेलन करना और हिन्दी या भारतीय भाषाओं का गुण बखान करना और बाकी वर्ष चुप रहना
(4) हिन्दी दिवस पर ऐसे हिन्दी साहित्यकार को पुरस्कृत करना जो कामकाज हिन्दी में नहीं करते (यह देखा गया कि हिन्दी दिवस पर सम्मानित साहित्यकार का पहचान पत्र पर केवल अंग्रेजी में था)।
(5) जब तक विभिन्न प्रदेश अंग्रेजी को अपने प्रदेश के जन जन के लिए खतरा नहीं समझते क्या तब तक अंग्रेजी की दासता से मुक्ति मिल सकती है?
(6) 40 प्रतिशत जनता अब भी अनपय्ढ है। अनपढ़ के लिए तो हिन्दी या अंग्रेजी समान है (7) जन जागरण द्वारा चुनावी मुद्दा बनाने के प्रयास नहीं, क्योंकि राजनेता तो केवल वोट की भाषा समझते हैं ।
हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं को प्रतिष्ठापित कराने के लिए संयुक्त प्रयास की अत्यंत आवश्यकतता है। इस प्रयास से पहले महामहिम राष्ट्रपति सहित सत्ता धारी वैज्ञानिकों एवं राजनेताओं के साथ निर्णायक चर्चा एवं जनसमुदाय के विचारों का सर्वेक्षण करना आवश्यक है कि अंग्रेजी का प्रयोग किस रूप, यथा माध्यम या विषय, में राष्ट्र एवं जन हित में है जिससे राष्ट्र में सबको समान अवसर मिल सकें और राष्ट्र आत्मनिर्भर होकर सवाभिमान से जी सके। यह भी विचारणीय है कि वर्तमान स्थिति से हम केवल उपभोक्ता बन रहे हैं और हम आधे अधूरे हो रहे हैं अर्थात न तो स्वभाषा पर हमारा अधिकार है और न ही अंग्रेजी पर।इस कार्य के लिए हमें लगातार लगे रहना होगा। गाजियाबाद संगोष्ठी में विभिन्न विचारों की समीक्षा करके कार्य योजना को पाँच वर्गों में बाँटने का प्रस्ताव रखा गया था। ये प्रस्ताव हैं सांसद एवं जन -जागरण, न्यायायिक प्रक्रिया, वैज्ञानिक-प्रौद्यौगिक-शिक्षा संबंधी प्रयास, साहित्य द्वारा जनजागरण, प्रतियोगिताओं द्वारा विचार मंथन,एवं जन आंदोलन। यह भी प्रस्ताव रखा गया कि निम्नलिखित भाषा नीति को लागू करवाने के प्रयास किए जाएं -
· संविधान के अनुसार देवनागरी लिपि में लिखी गई हिन्दी को भारत संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। राजभाषा हिन्दी को ही देश की सम्पर्क राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए।
· स्कूली शिक्षा का माध्यम मातृभाषा / प्रदेश की राज्यभाषा या जनभाषा हो। उच्च शिक्षा का माध्यम मातृभाषा / प्रदेश की राज्यभाषा या जनभाषा या सम्पर्क राष्ट्रभाषा हो। तकनीकी शब्दावली पूरे देश की एक हो। हर भारतीय को अष्टम सूची में मान्य भाषाओं में से दो भाषाएँ अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए उनमें से एक सम्पर्क राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए यदि हिन्दी सम्पर्क राष्ट्रभाषा है तो हिन्दी भाषियों को हिन्दी एवं संविधान में दी गई कोई भी प्रान्तीय एक भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए।
· राज्यों के सरकारी व राज्यस्तर के निजी संस्थाओं की कार्यभाषा अनिवार्य रूप से संविधान की अष्टम सूची में से कोई भी एक भाषा होनी चाहिए।
· किसी भी राज्य में राष्ट्रीय स्तर की निजी संस्थाओं तथा केन्द्र सरकार के हर राज्य में स्थित विभागों के कार्यालयों की कार्यभाषा अनिवार्य रूप से राष्ट्र की सम्पर्क भाषा एवं राज्य की राज्यभाषा हो।
· केन्द्र के ऐसे विभागों के कार्यालयों में,जो हर राज्य में स्थापित नहीं हैं, जैसे परमाणु ऊर्जा विभाग, संवाद की भाषा राष्ट्र की सम्पर्क भाषा हो व कर्मचारी अपना मूल लेखन अपनी राज्यभाषा/मातृभाषा में कर सकें और उसका अनुवाद सम्पर्क राष्ट्रभाषा में किया जाए।
हर राज्य में जन सेवा संबंधी सभी साधनों जैसे बस, रेल, टैक्सी, ऑटो इत्यादि तथा बैंकों, कार्यालयों, डाकघरों, दुकानों, फर्मों, संस्थानों आदि के सार्वजनिक सूचना बोर्र्डों पर स्थानीय लिपि के साथ देवनागरी लिपि का प्रयोग अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इसी प्रकार दवाइयों का नाम, घटक तथा प्रयोग विधि भी देवनागरी लिपि में हो। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर 'भारत में निर्मित' लिखा होना चाहिए, न कि made in India।
(डॉ विजय कुमार भार्गव
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय भाषा प्रतिष्ठापन राष्ट्रीय परिषद
एच 6/1 सेक्टर 7 वाशी नई मुंबई 400703)